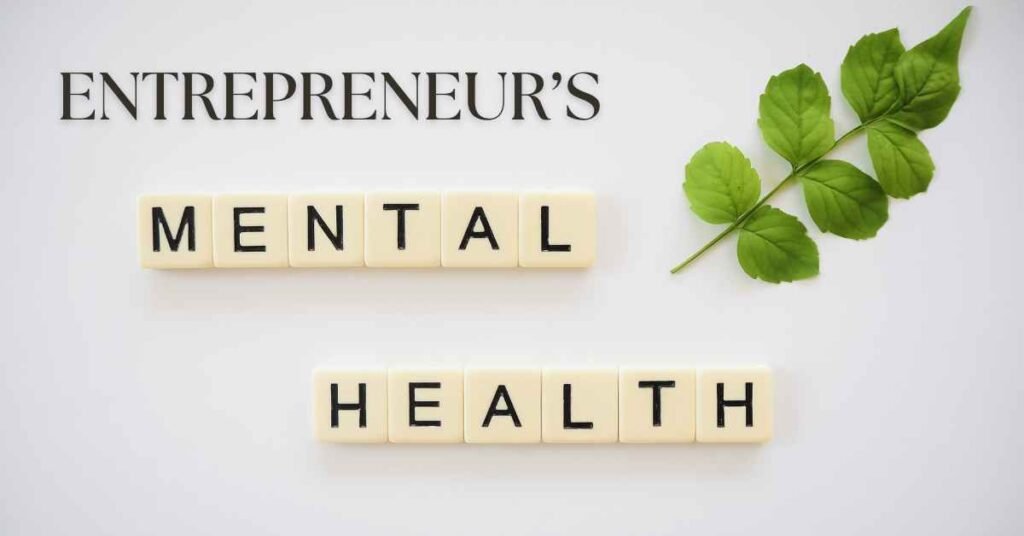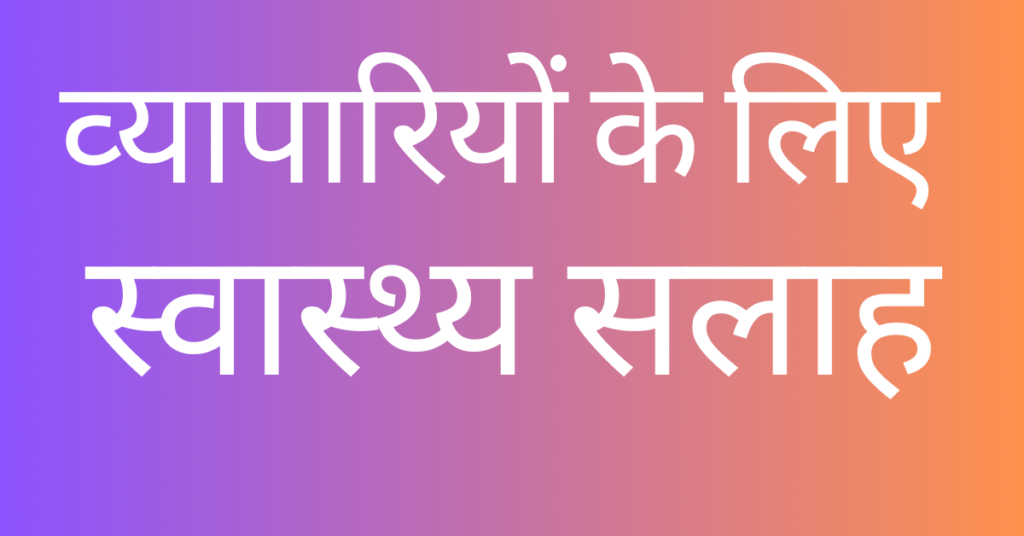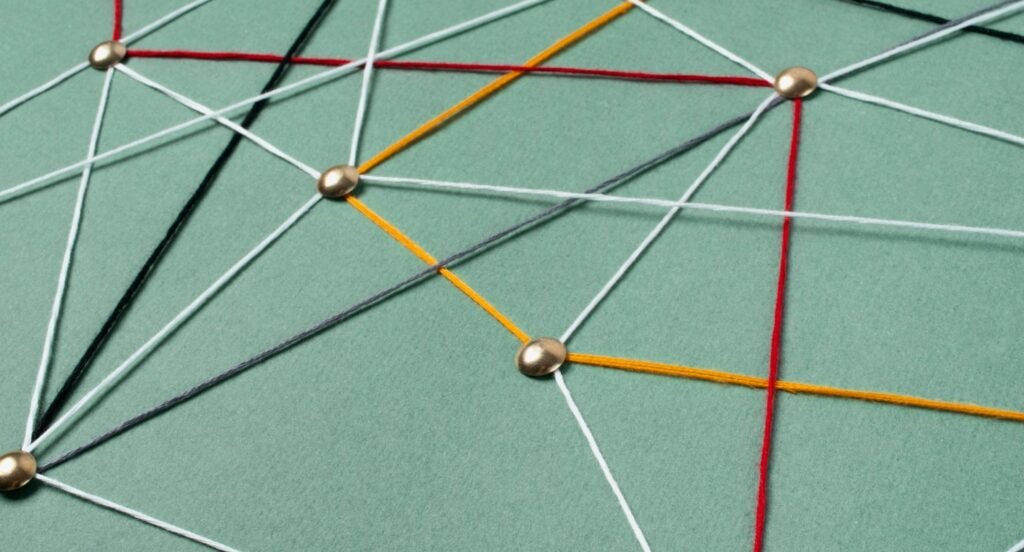
Designed by Freepik
Table of Contents
Toggleप्रस्तावना (Introduction)
संचार (Communication) किसी भी संगठन का आधार होता है। यह संगठन में कार्यप्रवाह, समझ, तालमेल और निर्णय प्रक्रिया को सहज बनाता है। संचार के विभिन्न प्रकारों में ऊर्ध्व संचार (Upward Communication), अधोमुखी संचार (Downward Communication), क्षैतिज संचार (Horizontal Communication) और तिर्यक संचार (Diagonal Communication) शामिल हैं। इनमें से तिर्यक संचार को अक्सर सबसे आधुनिक और लचीला संचार का रूप माना जाता है।
तिर्यक संचार का अर्थ है संगठन के अलग-अलग विभागों, अलग-अलग स्तरों और विभिन्न पदों के बीच सीधे संवाद की प्रक्रिया, जिसमें परंपरागत आदेश-श्रृंखला (Chain of Command) को दरकिनार कर, जरूरत के अनुसार संचार स्थापित किया जाता है।
तिर्यक संचार को विकर्ण संचार भी कहा जाता हैं।
तिर्यक संचार और विकर्ण संचार दोनो को अंग्रेजी भाषा में Diagonal Communication कहा जाता हैं।
इस लेख में हम संचार के इस प्रकार या type को तिर्यक और विकर्ण दोनों तरह के संचार कहने के बजाय सिर्फ तिर्यक संचार कहकर ही संबोधित करेंगे।
और जहां-जहां आवश्यकता हैं, वहां-वहां पर तिर्यक संचार के आगे कोष्ठक (Bracket) का उपयोग करेंगे और कोष्ठक में Diagonal Communication शब्द का उपयोग करेंगे।
इस लेख के अंत में तिर्यक संचार (Diagonal Communication) से सम्बंधित FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) भी दिए गए हैं।
FAQs में हम तिर्यक संचार के स्थान पर विकर्ण संचार शब्द का उपयोग करेंगे।
तिर्यक संचार की परिभाषा (Definition of Diagonal Communication)
तिर्यक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के किसी विभाग का कर्मचारी सीधे दूसरे विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी से संवाद करता है, चाहे उनके बीच पदानुक्रम (Hierarchy) का कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का उत्पादन प्रबंधक (Production Manager) सीधे वित्त विभाग के उप-प्रबंधक (Deputy Manager Finance) से बात करता है, तो यह तिर्यक संचार कहलाएगा। इसमें दोनों ही लोग अलग-अलग विभाग और अलग-अलग स्तरों से जुड़े होते हैं, लेकिन संवाद का उद्देश्य कार्य को तीव्र और प्रभावी बनाना होता है।
तिर्यक संचार की विशेषताएँ (Characteristics of Diagonal Communication)
पदानुक्रम से स्वतंत्रता – यह संचार औपचारिक आदेश श्रृंखला से बाहर होता है।
त्वरित संचार – समय की बचत होती है क्योंकि संदेश सीधे संबन्धित व्यक्ति तक पहुँचता है।
विभागों में तालमेल – विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ता है।
प्रभावशीलता – समस्या-समाधान और निर्णय-प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी हो जाती है।
संगठन की गतिशीलता – संगठन को बदलते परिवेश में अधिक लचीला बनाता है।
तिर्यक संचार के उदाहरण(Examples of Diagonal Communication)
एक मार्केटिंग मैनेजर का सीधे गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (Quality Control Department) के सुपरवाइजर से ग्राहक शिकायतों पर चर्चा करना।
मानव संसाधन विभाग का कोई अधिकारी (HR Executive) उत्पादन विभाग के किसी टीम लीडर से प्रशिक्षण संबंधी सुझाव साझा करना।
आईटी विभाग का कोई कर्मचारी सीधे वित्त विभाग के प्रबंधक से सॉफ़्टवेयर बजट पर विचार करना।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तिर्यक संचार में समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है।
तिर्यक संचार के लाभ (Advantages of Diagonal Communication)

समय की बचत – मध्यवर्ती स्तर (Intermediate Levels) से होकर संदेश ले जाने की आवश्यकता नहीं होती।
समस्या समाधान में तेजी – समस्याओं का तुरंत निवारण संभव हो जाता है।
बेहतर समन्वय – विभिन्न विभागों के बीच आपसी सहयोग और समझ बढ़ती है।
लचीलापन – बदलती परिस्थितियों में संगठन तुरंत निर्णय ले सकता है।
नवाचार को बढ़ावा – अलग-अलग विभागों के लोग आपस में विचार साझा कर नई योजनाएँ बना सकते हैं।
अनौपचारिक वातावरण का विकास – कर्मचारियों के बीच खुला संवाद और विश्वास बढ़ता है।
तिर्यक संचार की सीमाएँ (Limitations of Diagonal Communication)
औपचारिकता का अभाव – पारंपरिक पदानुक्रम टूटने से अनुशासन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन – कभी-कभी कर्मचारी अपने वरिष्ठों को दरकिनार कर सीधे दूसरे विभाग से संवाद करते हैं, जिससे टकराव हो सकता है।
सूचना की गलत व्याख्या – बिना आधिकारिक अनुमति के सीधे संवाद में गलतफहमी की संभावना बढ़ जाती है।
ईर्ष्या और असहमति – वरिष्ठ अधिकारियों को लग सकता है कि उनकी भूमिका को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
नियंत्रण में कठिनाई – जब हर विभाग और कर्मचारी स्वतंत्र रूप से संवाद करने लगे तो समग्र नियंत्रण कमजोर हो सकता है।
तिर्यक संचार बनाम अन्य संचार (Diagonal Communication Versus Other Types of Communication)
ऊर्ध्व संचार में अधीनस्थ अपने वरिष्ठ को सूचना देते हैं, जबकि तिर्यक संचार में किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति सीधे अन्य विभाग से जुड़ सकता है।
ऊर्ध्व संचार (Upward Communication): अर्थ, महत्व और उदाहरण
अधोमुखी संचार आदेश और निर्देशों के लिए प्रयोग होता है, जबकि तिर्यक संचार अधिकतर सहयोग और समस्या-समाधान पर केंद्रित होता है।
अधोमुखी संचार (Downward Communication): अर्थ, महत्व, उदाहरण
क्षैतिज संचार समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है, जबकि तिर्यक संचार में स्तर और विभाग दोनों बदल जाते हैं।
क्षैतिज संचार (Lateral Communication): अर्थ, महत्व और उदाहरण
आधुनिक संगठनों में तिर्यक संचार का महत्व (The Importance of Diagonal Communication in Modern Organizations)
आज के प्रतिस्पर्धी और गतिशील व्यावसायिक परिवेश में संगठन को तेजी से निर्णय लेना पड़ता है। परंपरागत ऊर्ध्व और अधोमुखी संचार में अक्सर समय बर्बाद होता है। ऐसे में तिर्यक संचार संगठन को फुर्तीला और नवाचार के लिए सक्षम बनाता है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ – विभिन्न देशों और विभागों के बीच सीधे संवाद की आवश्यकता होती है।
आईटी कंपनियाँ – त्वरित समाधान और तकनीकी सहयोग के लिए तिर्यक संचार आवश्यक है।
स्टार्टअप्स – सीमित संसाधनों में तेज़ निर्णय और विभागों में तालमेल के लिए यह सबसे उपयोगी तरीका है।
तिर्यक संचार को प्रभावी बनाने के उपाय (Measures to Make Diagonal Communication Effective)
स्पष्ट नीतियाँ बनाना – संगठन को यह तय करना चाहिए कि तिर्यक संचार किन परिस्थितियों में अनुमत होगा।
वरिष्ठों की सहमति – संवाद इस प्रकार होना चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को नज़रअंदाज़ न किया जाए।
सूचना का दस्तावेजीकरण – गलतफहमी से बचने के लिए संवाद को लिखित रूप में संजोना आवश्यक है।
प्रशिक्षण – कर्मचारियों को सही संचार कौशल और पेशेवर व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता बनाए रखना – ताकि विभागों और अधिकारियों के बीच विश्वास की कमी न हो।
निष्कर्ष (Conclusion)
तिर्यक संचार (Diagonal Communication) आधुनिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण संचार शैली है। यह परंपरागत पदानुक्रम से हटकर तेज़, प्रभावी और सहयोगी संवाद की सुविधा प्रदान करता है। यद्यपि इसमें अनुशासन, नियंत्रण और अधिकार संबंधी चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन यदि इसे सुव्यवस्थित ढंग से अपनाया जाए तो यह संगठन की उत्पादकता, नवाचार और लचीलापन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा तीव्र है और हर संगठन को तेजी से निर्णय लेने पड़ते हैं, तिर्यक संचार संगठन की सफलता की कुंजी बन सकता है।
Diagonal Communication – FAQs (विकर्ण संचार : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
विकर्ण संचार (Diagonal Communication) क्या है?
विकर्ण संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के विभिन्न विभागों और अलग-अलग स्तरों के कर्मचारियों के बीच सीधे संचार होता है।
विकर्ण संचार को विकर्ण क्यों कहा जाता है?
क्योंकि यह न तो पूरी तरह ऊर्ध्वाधर होता है और न ही क्षैतिज, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है, जो संगठन संरचना में तिरछी (Diagonal) दिशा में चलता है।
विकर्ण संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य तेजी से सूचना साझा करना, समन्वय बढ़ाना और कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना होता है।
विकर्ण संचार के सामान्य उदाहरण क्या हैं?
किसी विभाग का मैनेजर दूसरे विभाग के कर्मचारी से सीधे बात करे, या प्रोजेक्ट टीम में अलग-अलग स्तरों के सदस्य आपस में संवाद करें।
विकर्ण संचार क्यों महत्वपूर्ण है?
यह निर्णय लेने की गति बढ़ाता है, विभागीय बाधाएँ कम करता है और टीमवर्क को मजबूत बनाता है।
विकर्ण संचार के प्रमुख लाभ क्या हैं?
बेहतर समन्वय, तेज़ समस्या समाधान, प्रभावी सूचना प्रवाह और कार्यक्षमता में वृद्धि इसके प्रमुख लाभ हैं।
विकर्ण संचार की सीमाएँ क्या हैं?
यदि नियंत्रण न हो तो यह अधिकारों में भ्रम, अनुशासनहीनता और टकराव का कारण बन सकता है।
विकर्ण संचार और क्षैतिज संचार में क्या अंतर है?
क्षैतिज संचार समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है, जबकि विकर्ण संचार अलग-अलग स्तर और विभागों के बीच होता है।
संगठन में विकर्ण संचार को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है?
स्पष्ट भूमिका निर्धारण, खुले संवाद की संस्कृति और उचित दिशा-निर्देशों से विकर्ण संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है।
आधुनिक संगठनों में विकर्ण संचार का क्या महत्व है?
आधुनिक, मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट-आधारित संगठनों में विकर्ण संचार नवाचार और तेजी से काम पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।