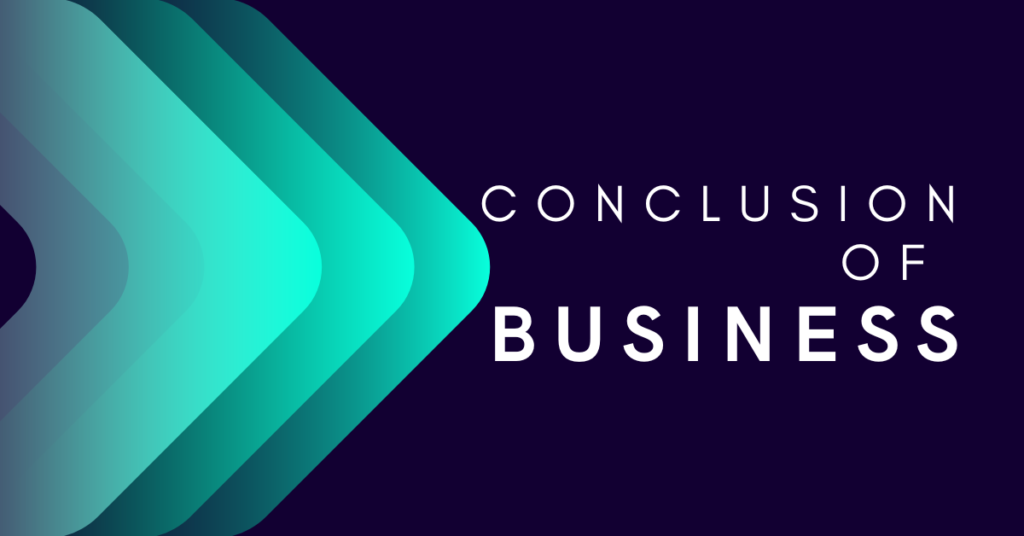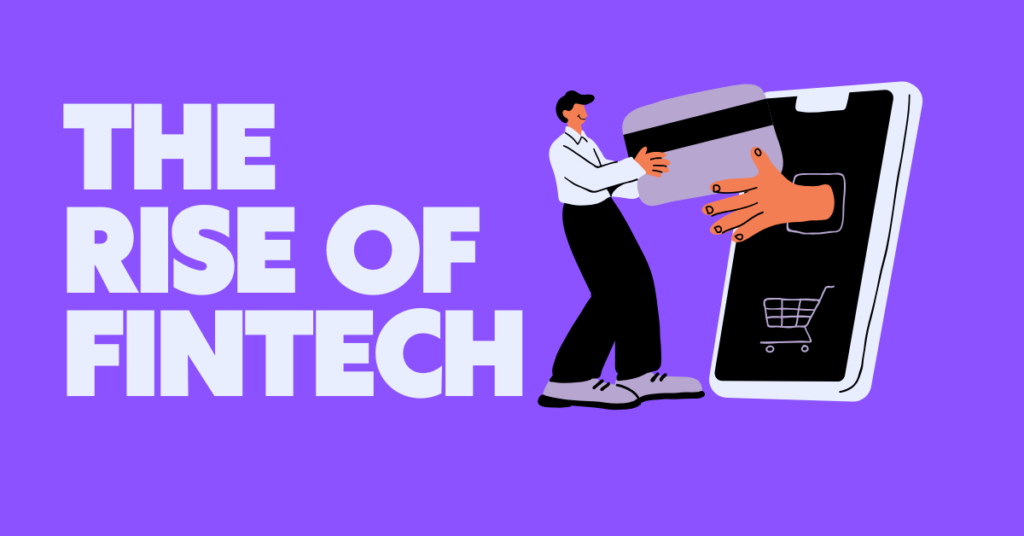Designed by Freepik
Table of Contents
Toggleप्रस्तावना
व्यवसाय के संचालन और विकास के लिए पूंजी (Capital) की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन की वित्तीय मजबूती और दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपनी पूंजी का प्रबंधन और संयोजन किस प्रकार किया है। यही संयोजन पूंजी संरचना (Capital Structure) कहलाता है।
पूंजी संरचना उस अनुपात को दर्शाती है जिसमें कोई कंपनी ऋण (Debt) और इक्विटी (Equity) के माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। सरल शब्दों में, यह बताती है कि व्यवसाय अपनी पूंजी कहाँ से और किस प्रकार जुटाता है।
पूंजी संरचना की परिभाषा
जे. एफ. ब्रैडली (J.F. Bradley) के अनुसार –
“पूंजी संरचना का आशय उस पूंजी के अनुपात से है जो दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी पूंजी के बीच होता है।”गेरस्टेनबर्ग (Gerstenberg) के अनुसार –
“पूंजी संरचना किसी कंपनी द्वारा उपयोग किए गए दीर्घकालिक पूंजी स्रोतों का मिश्रण है।”
संक्षेप में, पूंजी संरचना का अर्थ है – इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, डिबेंचर, बांड और दीर्घकालिक ऋण का वह सम्मिश्रण, जिसके माध्यम से कंपनी अपनी दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत पूरी करती है।
पूंजी संरचना के प्रमुख घटक
पूंजी संरचना में विभिन्न वित्तीय साधनों का समावेश होता है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं –
1. इक्विटी शेयर पूंजी (Equity Share Capital)
कंपनी की स्वामित्व पूंजी।
शेयरधारक कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं।
इक्विटी शेयरधारक लाभांश (Dividend) प्राप्त करते हैं, परंतु यह सुनिश्चित नहीं होता।
जोखिम अधिक परंतु प्रतिफल भी अधिक हो सकता है।
2. वरीयता शेयर पूंजी (Preference Share Capital)
इसमें निवेशक को एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है।
इक्विटी की तुलना में कम जोखिम।
कंपनी के परिसमापन (Liquidation) के समय वरीयता शेयरधारकों को इक्विटी से पहले भुगतान मिलता है।
3. ऋण (Debt) या डिबेंचर (Debentures)
यह उधार ली गई पूंजी है।
डिबेंचर धारकों को निश्चित ब्याज (Interest) प्राप्त होता है।
कंपनी के दिवालिया होने पर डिबेंचर धारकों को प्राथमिकता से भुगतान किया जाता है।
4. अवितरित लाभ (Retained Earnings)
कंपनी द्वारा अर्जित मुनाफे का वह हिस्सा, जिसे लाभांश के रूप में वितरित न करके पुनः व्यवसाय में लगाया जाता है।
यह आंतरिक स्रोत है और बाहरी दायित्व नहीं पैदा करता।
5. दीर्घकालिक ऋण (Long-term Loans)
बैंक और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण।
इन पर ब्याज देना होता है।
पूंजी संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
पूंजी संरचना के प्रकार
1. सरल पूंजी संरचना (Simple Capital Structure)
इसमें केवल इक्विटी शेयर और अवितरित लाभ का उपयोग होता है।
कोई जटिल ऋण या वरीयता पूंजी नहीं होती।
2. जटिल पूंजी संरचना (Complex Capital Structure)
इसमें इक्विटी, वरीयता शेयर, डिबेंचर, ऋण और अन्य साधन सम्मिलित होते हैं।
यह अधिकतर बड़ी कंपनियों में प्रचलित है।
पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक
किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना कई आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं –
- व्यवसाय का स्वभाव (Nature of Business)
- सेवा-आधारित कंपनियाँ सामान्यतः ऋण पर कम निर्भर रहती हैं।
- पूंजी-गहन उद्योग जैसे – स्टील, सीमेंट अधिक ऋण लेते हैं।
- व्यवसाय का आकार (Size of Business)
- बड़ी कंपनियाँ विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटा सकती हैं।
- छोटी कंपनियाँ मुख्य रूप से इक्विटी या बैंक ऋण पर निर्भर होती हैं।
- लाभ की स्थिरता (Stability of Earnings)
- स्थिर और नियमित मुनाफा कमाने वाली कंपनियाँ अधिक ऋण ले सकती हैं।
- अस्थिर मुनाफे वाली कंपनियाँ इक्विटी पर निर्भर रहती हैं।
- बाजार की स्थिति (Market Conditions)
- मंदी के समय इक्विटी जारी करना कठिन होता है।
- उछाल के समय इक्विटी निवेशक आसानी से मिल जाते हैं।
- कर नीति (Tax Policy)
- ऋण पर ब्याज कर में छूट योग्य होता है।
- इससे कंपनियाँ ऋण को प्राथमिकता देती हैं।
- नियंत्रण का पहलू (Control Consideration)
- यदि मालिकाना हक बनाए रखना है तो कंपनी ऋण लेगी, न कि अधिक इक्विटी जारी करेगी।
- लचीलापन (Flexibility)
- पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी आवश्यकता अनुसार जल्दी से परिवर्तन कर सके।
कॉर्पोरेट फाइनेंस (Corporate Finance): परिभाषा, महत्व, कार्य
आदर्श पूंजी संरचना (Ideal Capital Structure)
आदर्श पूंजी संरचना वह है जिसमें –
जोखिम और प्रतिफल का संतुलन हो।
पूंजी की लागत (Cost of Capital) न्यूनतम हो।
कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता बनी रहे।
नियंत्रण (Control) संतुलित रहे।
लचीलापन (Flexibility) हो।
पूंजी संरचना के सिद्धांत
1. शुद्ध आय सिद्धांत (Net Income Theory)
मानता है कि पूंजी संरचना में ऋण का अनुपात बढ़ाने से कंपनी का मूल्य बढ़ता है।
क्योंकि ऋण पर ब्याज कर से छूट योग्य होता है।
2. शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत (Net Operating Income Theory)
मानता है कि पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कंपनी का मूल्य उसकी आय पर निर्भर करता है।
3. पारंपरिक सिद्धांत (Traditional Theory)
मानता है कि एक संतुलित पूंजी संरचना होती है।
कुछ हद तक ऋण बढ़ाने से कंपनी का मूल्य बढ़ता है, लेकिन अधिक ऋण से जोखिम भी बढ़ जाता है।
4. मोडिग्लियानी-मिलर सिद्धांत (Modigliani and Miller Theory)
इनके अनुसार, यदि कर न हो तो पूंजी संरचना का कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
परंतु वास्तविक परिस्थितियों में कर और जोखिम के कारण पूंजी संरचना का महत्व होता है।
पूंजी संरचना के लाभ
कर लाभ (Tax Advantage):
ऋण पर ब्याज कर में कटौती योग्य होता है।लागत में कमी (Reduction in Cost of Capital):
उचित मिश्रण से पूंजी की औसत लागत कम होती है।शेयरधारकों के प्रतिफल में वृद्धि (Increase in Shareholders’ Return):
सही संरचना से इक्विटी पर अधिक लाभांश मिल सकता है।विकास की सुविधा (Growth Facilitation):
उचित संरचना से कंपनी को विस्तार में आसानी होती है।
पूंजी संरचना के हानियाँ
अत्यधिक ऋण का जोखिम (Risk of Over-leverage):
अधिक ऋण से दिवालिया होने की संभावना बढ़ जाती है।लचीलापन कम होना (Reduced Flexibility):
अत्यधिक निश्चित दायित्व होने पर कंपनी की स्वतंत्रता कम हो जाती है।नियंत्रण का ह्रास (Loss of Control):
अधिक इक्विटी जारी करने पर मालिकाना हक कमजोर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
पूंजी संरचना किसी भी कंपनी की वित्तीय रीढ़ होती है। यह कंपनी की जोखिम वहन क्षमता, लागत, लाभ और नियंत्रण सभी को प्रभावित करती है। एक आदर्श पूंजी संरचना न केवल पूंजी की लागत को कम करती है, बल्कि कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करती है।
अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय – जोखिम, लागत, नियंत्रण और लचीलापन – सभी पहलुओं का संतुलित ध्यान रखें।